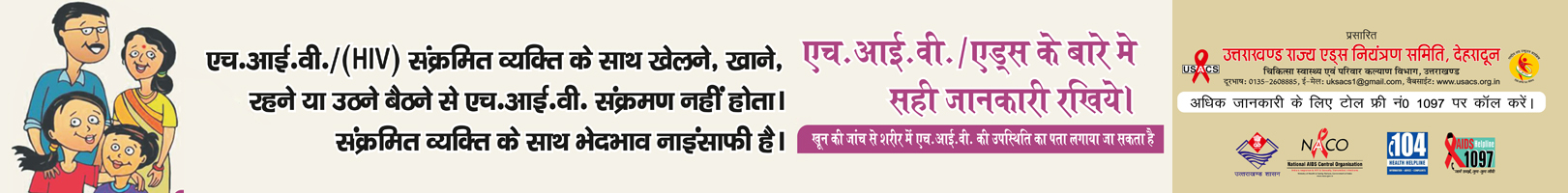देश के पाँच राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव नें एक बार फिर ‘आया राम और गया राम’ का वीभत्स नृत्य शुरु कर दिया है। असली ताण्डव होगा चुनावों के नतीजों के स्वरूप पर जब सरकार बनने की स्थिति आयेगी। छोटी विधानसभाओं में दल-बदल और भी आसान होता है जहां एक या दो सदस्यो के ख़रीद-फ़रोख़्त व दल बदल से सरकारे बनती और बिगड़ती हैं। चुनाव से पूर्व उत्तराखंड में कई विधायकों और नेताओं ने दल बदले, कोई पार्टी से निष्कासित किये गये तो कुछ टिकट न मिलने से नाराज़ होकर विपक्ष में चले गये। परन्तु अब निर्वाचको पर ही निर्भर है कि वे दल बदलुओं को विजयी करते है या परास्त। दल बदल को रोकने के लिए संसद ने 1985 में 52वें सविंधान संशोधन द्वारा सविंधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी जिसे 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा और कठोर बनाया गया। संवैधानिक स्थिति अब यह है कि विधायिका का सदस्य, चाहे वह संसद या राज्य विधानमंडल का हो, अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य है। दसवीं अनुसूची के अनुसार किसी विधायक को अयोग्य ठहराने के आधार हैं, यदि उसने स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है, या, यदि वह सदन में मतदान के समय अनुपस्थित रहता है या अपने दल के दिशा-निर्देश के विपरीत मतदान करता है। हालांकि, विधायक दल के सदस्यों के दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय करते हैं तो दलबदल-विरोधी कानून लागू नहीं होगा। अयोग्यता के सवाल पर निर्णय के लिँये सक्षम पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष / सभापति होते हैं जिनके निर्णय की, किहोटो होलोहन बनाम ज़चिल्हू और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, 1992, न्यायिक समीक्षा ही हो सकती है।
प्रत्येक राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए तथा आन्तरिक अनुशासन रखनें के लिए अपने पार्टी के संविधान के तहत सशक्त है। इसमें कोई शक नहीं कि अनुशासन के बिना राजनीतिक दल सत्ता के भूखे लोगों की भीड़ रह जायेगी। संसदीय लोकतन्त्र में हरेक दल की एक सुचिन्तित विचारधारा और राजनीतिक पहचान अपेक्षित है जिसके अाधार पर वे जनादेश प्राप्त करते हैं। राजनीतिक दल खुद अपनी पार्टी को कैसे अनुशासित करते हैं – यह उनका आंतरिक मामला है। एक अखिल भारतीय राजनीतिक पार्टी में, स्वाभाविक रूप से, उच्च पदों के लिए नेताओं के बीच आंतरिक संघर्ष होगा। आखिरकार, यह योग्यतम का अस्तित्व है, यानी जो नेता पार्टी के भीतर अधिकतम समर्थन हासिल करता है, वही शीर्ष स्थान पर आसीन होगा। फिर भी कोई भी नेता लंबे समय तक शीर्ष स्थान पर टिक नही सकता है यदि वह निरंकुश है और यदि वह अपने सहयोगियों और पार्टी के पदाधिकारियों के सम्मान व गरिमा को ठेस पहुँचाता है। ‘सत्ता हासिल करना,मानव जाति का एक सामान्य स्वभाव है–एक सतत, बेचैन इच्छा- जो केवल मृत्यु के साथ खत्म होती है।’ दलबदल विरोधी कानून राजनीतिक महत्वाकांक्षा के विरुद्ध नहीं है, वह केवल दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाना चाहता है। यह राजनीतिक दलो का दायित्व है कि अपनी पार्टी में लोकतन्त्र के सिद्धान्तो का अनुसार करते हुए पार्टी में आन्तरिक अनुशासन रखें और यह भी सुनिश्चित करें की पार्टी के सदस्य विशेषकर जो उच्चपदो पर हैं पार्टी या सरकार में वे पार्टी के सिद्धान्तों और दर्शन का अनुपालन करें जो इस बात का प्रमाण है कि एक राजनीतिक दल दूसरे दल से विभिन्न पहचान रखता है। वर्तमान के परिपेक्ष में तो, विशेषकर, व्यापक दल-बदल के कारण राजनीतिक दलो की विशिष्ठ पहचान नेपथ्य में विलीन हो गई है और एक मात्र उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति बन गया है।
इस सन्दर्भ में मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटना क्रम और उलट फेर का उल्लेख प्रासंगिक है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा जब यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें विधानसभा में बहुमत का खो दिया है। जो हुआ वह अकल्पनीय था लेकिन इसकी जड़ें मुख्यमंत्री की निरंकुश और गुटीय राजनीति में थीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से असंतुष्ट होकर “बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार” का आरोप लगाया और अपने वफादार 22 विधायकों के साथ विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इससे कमलनाथ सरकार का पतन और भाजपा के शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी हुई। सिंधिया बाद में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। 22 सिंधिया वफादारों में से, 14 विधायक, जिन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, को दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री सहित 34 मंत्रियों में से14 सिंधिया निष्ठावान थे। बाद में ये सभी निर्वाचित हो गये विधान सभा के सदस्य। उल्लेखनीय है कि संविधान में एक व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद में प्रतिभा को शामिल करने के लिए किसी प्रतिभावान व्यक्ति को मन्त्री बनाया जा सकता है यदि वह पात्र हो। ऐसे व्यक्ति को छह महीने के अन्दर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा अन्यथा वह मन्त्रिपरिषद का सदस्य नहीं रहेगा। अतीत में कई उदाहरण हैं, विशेष रूप से केंद्रीय स्तर पर, जब गैर-सदस्यों को मंत्री बनाया गया और बाद में उन्हें लोकसभा या राज्यसभा के लिए चुना गया। उदाहरण के लिए, पीवी नरसिम्हा राव तब संसद सदस्य (सांसद) नहीं थे, जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बाद में वह आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के नंदयाल से चुनाव लड़े और लोकसभा के लिए चुने गए। इसी तरह, देवेगौड़ा सांसद नहीं थे, जब उन्होंने 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह राज्यसभा के लिए चुने गए थे। फरवरी 1995 में, प्रणब मुखर्जी, तब सांसद नहीं थे, उन्हें मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी और उन्होंने कुछ समय के लिए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, लेकिन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के साथ खींचतान के कारण संसद के लिए निर्धारित अवधि के अन्दर निर्वाचित नहीं हो सके। मुखर्जी को इस्तीफा देना पड़ा और बाद में उन्हें नरसिम्हा राव द्वारा योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सुब्रह्मण्यम जयशंकर को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और बाद में उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। उद्धव ठाकरे भी बाद में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बनें।
लेकिन मध्य प्रदेश में, इस सविंधानिक व्यवस्था का उपयोग राजनीतिक दरार को बढ़ावा देने, विभाजन करने और एक निर्वाचित सरकार के पतन के के लिए थोक में उपयोग में लाया गया जिसका कोई पूर्व उदाहरण नही है। जाहिर है, वहाँ दल बदल कानून की अवहेलना नहीं हुई, सीमित कानूनी दलील की दृंष्ठि से। लेकिन सवाल उससे बहुत बड़ा और व्यापक है, दल बदल कानून निर्माताओं की मनसा और संविधानिक मर्यादा की। संविधान का 52वां संशोधन दलबदल की बुराई और ‘आया राम गया राम’ की राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था ताकि मतदाताओं के मतदान का सौदा न हो और संसदीय लोकतंत्र की नींव स्थिर और मज़बूत रहे।
दलबदल-विरोधी कानून की पुन: समीक्षा होनी चाहिए और कानून में यह व्यवस्था हो कि मंत्री बनने से पहले विधायिका की सदस्यता आवश्यक हो और जो सदस्य दल बदल करता है किसी चुनाव जीतने के बाद उसे अगले पाँच वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया जाय। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाता अपने विवैक से ‘मतदान’ करें ताकि ऐसे प्रत्याशी विजयी हो जो अपनी राजनीतिक दल की विचारधारा से ओतप्रोत हों, जनसेवा ही जिनका सुस्पष्ट जीवन उद्देश्य और लक्ष्य हो, जो उज्जवल छवि के हों और पारिवारिक मोह से ग्रस्त न हों। संसद तो केवल क़ानून ही बना सकती है और जो बने भी है परन्तु दल-बदलु तो माहिर होते है अपने मनतव्य में और दल-बदल क़ानून अक्सर मजबूर और अप्रभावी रहा है। सारा दारोमदार अब मतदाताओं पर है जो मतदान करेंगे बिना किसी लोकलुभावन के। निःसन्देह हमारा गणतन्त्र उत्तरोत्तर स्रेयसकर बनेगा मतदाताओं के विवेकपूर्ण मतदान से ही और उत्तराखण्ड इस दिशा में अग्रणी भूमिका अदा करेगा।
(लेखक पूर्व अपर सचिव लोकसभा हैं और संवैधानिक और संसदीय मामलों के विशेषज्ञ। उल्लिखित विचार निजि हैं।)